कामाल चौधरी ने गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर और महाकवि नज़रुल से प्रेम किया है और बंगलादेश के मुक्ति-संग्राम के आल्हाद और अवसाद को जिया है। उनकी कविताओं का कथ्य और शिल्प हमारे देश के नई कविता आंदोलन जैसा लगता है, लेकिन उनमें आत्मनिर्वासन, अकेलापन, अजनबीपन, घुटन, कुंठा, निराशा, संत्रास, सड़न, बदबू जैसी क्षणजीवी नकारात्मक आधुनिक भावबोध की प्रवृत्तियां नहीं हैं। वे सकारात्मक आधुनिक भावबोध के कवि हैं। उनका सौंदर्यबोध ज़मीन पर सीधे खड़े रहकर क्षितिज देखता है और मानता है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। अजनबी नहीं होता। उसके जीवन में सड़न, घुटन, निराशा नहीं होती। बशर्ते हम इतिहास में बहाए गए ख़ून से सनी लाइनों के ख़तों को पढ़ना सीख लें। वे मानते हैं कि समाज, संसार, लड़ाइयां और राष्ट्रसंघ द्वारा पोषित हथियारों के गोदाम हमारे बाजू में राहत की पट्टी नहीं, नफ़रत के घाव बांधते हैं। ज़िंदगी एक टुकड़ा लकड़ी के क्रैच पर घिसटती है, इसलिए वे बार-बार अपनी स्वयं की महत्ता पहचानने का आह्वान करते हैं और बताते हैं कि मेहनती पसीने की खुशबू हमारी मृगनाभि सुगंध है। पसीने की खुशबू से ज़्यादा बेहतर खुशबू संसार में नहीं है। उनकी कविता अवसादग्रस्त मानव का संबल बनती है। इंसानियत के सशक्तिकरण के लिए वे अपनी कविता से ‘चंद बेख़ौफ़ मज़दूर’ लेने का प्रस्ताव रखते हैं। सलाह देते हैं कि ‘गाने गाओ नजरुल के, एक बार गाने गा कर तो देखो।‘कुल मिलाकर प्रगतिशील काव्यांदोलन और बांग्ला साहित्य की विकसित चेतना की सुदृढ़ परंपरा के साथ वे अपनी कविताओं में आज के समाज को दलदली अंधेरे से निकालने की कोशिश करते हैं। खरा बोलने के अपने ख़तरे हैं, फिर भी बोलना तो होगा ही, वे कहते हैं ‘अगर मैं बोलूं तो हड्डियों में होता है शहंशाही दर्द।‘ अब ये शहंशाही दर्द क्या है, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो इन कविताओं से गुज़रिए, पढ़िए, क्योंकि अगर आप इनसे रूबरू नहीं हुए तो ये बीच में से उठकर किसी रिफ्यूजी गली में घर ढूंढने के लिए नींद में चली जाएंगी।
कामाल चौधुरी की कविताएं
कामाल चौधरी ने गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर और महाकवि नज़रुल से प्रेम किया है और बंगलादेश के मुक्ति-संग्राम के आल्हाद और अवसाद को जिया है। उनकी कविताओं का कथ्य और शिल्प हमारे देश के नई कविता आंदोलन जैसा लगता है, लेकिन उनमें आत्मनिर्वासन, अकेलापन, अजनबीपन, घुटन, कुंठा, निराशा, संत्रास, सड़न, बदबू जैसी क्षणजीवी नकारात्मक आधुनिक भावबोध की प्रवृत्तियां नहीं हैं। वे सकारात्मक आधुनिक भावबोध के कवि हैं। उनका सौंदर्यबोध ज़मीन पर सीधे खड़े रहकर क्षितिज देखता है और मानता है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। अजनबी नहीं होता। उसके जीवन में सड़न, घुटन, निराशा नहीं होती। बशर्ते हम इतिहास में बहाए गए ख़ून से सनी लाइनों के ख़तों को पढ़ना सीख लें। वे मानते हैं कि समाज, संसार, लड़ाइयां और राष्ट्रसंघ द्वारा पोषित हथियारों के गोदाम हमारे बाजू में राहत की पट्टी नहीं, नफ़रत के घाव बांधते हैं। ज़िंदगी एक टुकड़ा लकड़ी के क्रैच पर घिसटती है, इसलिए वे बार-बार अपनी स्वयं की महत्ता पहचानने का आह्वान करते हैं और बताते हैं कि मेहनती पसीने की खुशबू हमारी मृगनाभि सुगंध है। पसीने की खुशबू से ज़्यादा बेहतर खुशबू संसार में नहीं है। उनकी कविता अवसादग्रस्त मानव का संबल बनती है। इंसानियत के सशक्तिकरण के लिए वे अपनी कविता से ‘चंद बेख़ौफ़ मज़दूर’ लेने का प्रस्ताव रखते हैं। सलाह देते हैं कि ‘गाने गाओ नजरुल के, एक बार गाने गा कर तो देखो।‘कुल मिलाकर प्रगतिशील काव्यांदोलन और बांग्ला साहित्य की विकसित चेतना की सुदृढ़ परंपरा के साथ वे अपनी कविताओं में आज के समाज को दलदली अंधेरे से निकालने की कोशिश करते हैं। खरा बोलने के अपने ख़तरे हैं, फिर भी बोलना तो होगा ही, वे कहते हैं ‘अगर मैं बोलूं तो हड्डियों में होता है शहंशाही दर्द।‘ अब ये शहंशाही दर्द क्या है, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो इन कविताओं से गुज़रिए, पढ़िए, क्योंकि अगर आप इनसे रूबरू नहीं हुए तो ये बीच में से उठकर किसी रिफ्यूजी गली में घर ढूंढने के लिए नींद में चली जाएंगी।
| Published Year | 2003 |
|---|---|
| Page Count | 160 |
| ISBN | 32546987137 |
| Author |
तपन मजूमदार |
| Publisher |
Rubric Publishing |
Editorial Review
From Publishers Weekly
In Golemon's so-so third Event Group thriller (after 2007's Legend), the shadowy U.S. government organization specializing in paranormal assignments, led by military maverick Col. Jack Collins, must stop the descendants of 2,000 children who survived the sinking of Atlantis 11,000 years earlier from seizing a key that will enable them to manipulate the tectonic plates of the earth's crust. After Collins's team finds a map of the lost continent during a raid on a mansion in Katonah, N.Y., the Atlanteans retaliate by slaughtering the FBI agent working with Collins as well as Event Group members manning the storage facility where the raid's spoils were being studied. The formulaic fight scenes, betrayals and 11th-hour rescues are on a par with the implausible premise. Even the dramatic conclusion will leave many readers unaffected.(Aug.)
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
From Booklist
Golemon’s third novel in the Event Group series proves to be his best yet. The Event Group is a secret military organization that specializes in the retrieval and study of ancient technology. The premise this time is elaborate: more than 10,000 years ago, the citizens of Atlantis developed a weapon so powerful that it destroyed their civilization and led to the story of Noah’s flood. The device they used is now in the hands of a society that traces their lineage back to the dynasty of Caesar. Colonel Jack Collins and his team must stop the group from using the superweapon and unleashing massive devastation. The resulting tale is a mix of the James Rollins action-heavy adventure, the military gadgetry of Tom Clancy, the pacing of the television series 24, and the conspiracy theories devoured by fans of the radio show Coast to Coast AM. For no-frills adventure fans with a taste for over-the-top plots. --Jeff Ayers --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

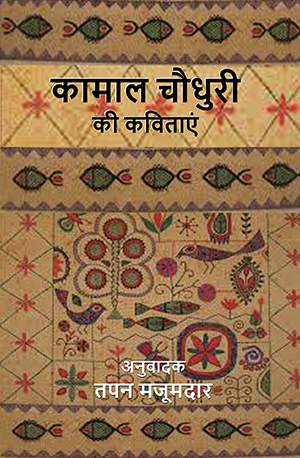

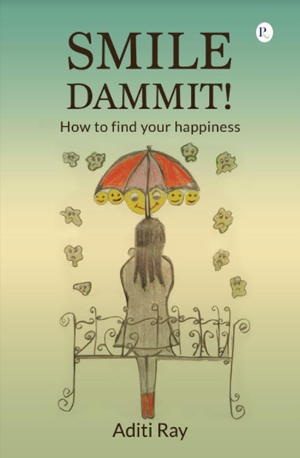
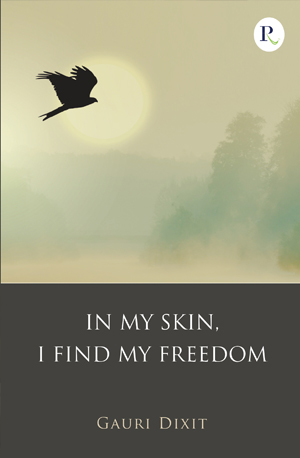
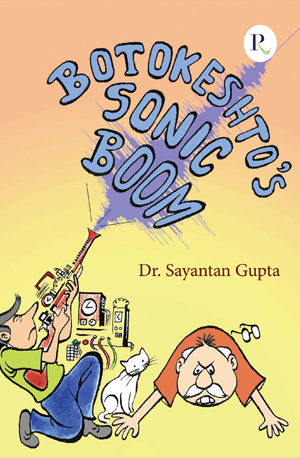
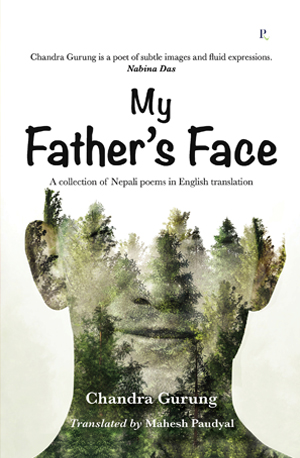
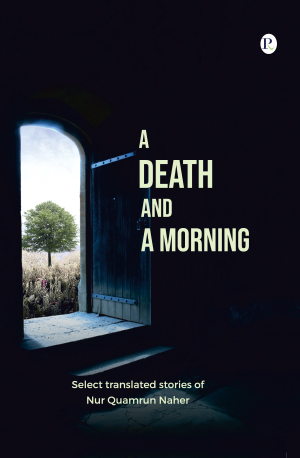
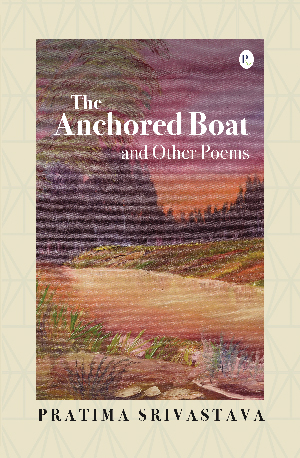
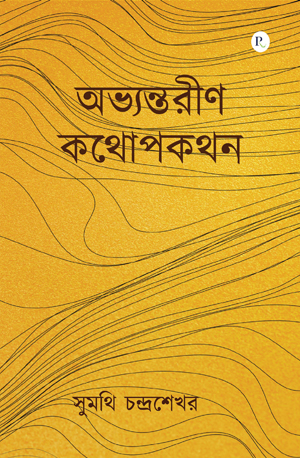

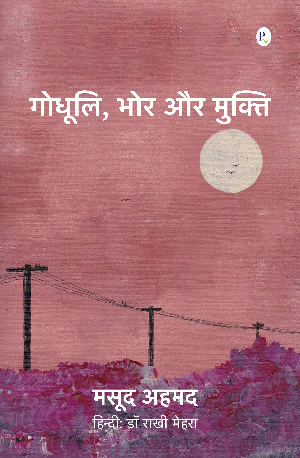
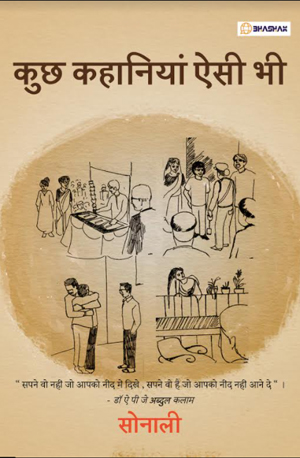
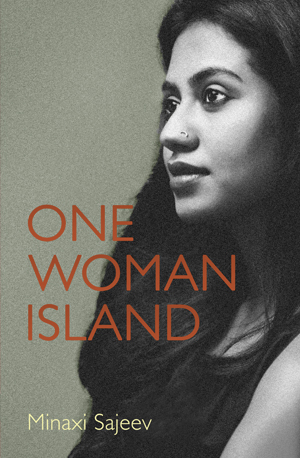
Reviews
There are no reviews yet.